असंभव क्रांति-(साधना-शिविर)
साधना-शिविर माथेरान, दिनांक 20-10-67 सुबह
(अति-प्राचिन प्रवचन)
प्रवचन-पांचवां-(क्रांति का क्षण)
मेरे
प्रिय आत्मन्,
एक
बहुत पुरानी कथा है। किसी पहाड़ की दुर्गम चोटियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था।
उस गांव का कोई संबंध,
वृहत्तर मनुष्य जाति से नहीं था। उस गांव के लोगों को प्रकाश कैसे
पैदा होता है, इसकी कोई खबर न थी।
लेकिन
अंधकार दुखपूर्ण है,
अंधकार भयपूर्ण है, अंधकार अप्रीतिकर है,
इसका उस गांव के लोगों को भी बोध होता था। उस गांव के लोगों ने
अंधकार को दूर करने की बहुत चेष्टा की। इतनी चेष्टा की कि वे अंधकार को दूर करने
के प्रयास में करीब-करीब समाप्त ही हो गए। वे रात को टोकरियों में भरकर अंधकार को
घाटियों में फेंक आते। लेकिन पाते कि टोकरियां भरकर फेंक भी आए हैं, फिर भी अंधकार अपनी ही जगह बना रहता है।
उन्होंने
बहुत उपाय किए। वह पूरा गांव पागल हो गया अंधकार को दूर करने के उपायों में।
अंधकार को धक्के देने की कोशिश करते, तलवारों, लाठियों
से अंधकार को धमकाते। लेकिन अंधकार न उनकी सुनता, न उनसे
हटता, न उनसे मिटता। और अंधकार को मिटाने की कोशिश में और
बार-बार हार जाने के कारण वे इतने दीन-हीन, इतने दुखी,
इतने पीड़ित हो गए कि उन्हें जीवन में कोई रस, जीवन
में कोई आनंद फिर दिखाई नहीं पड़ता था। एक ही बात दिखाई पड़ती थी कि शत्रु की तरह
अंधकार खड़ा है और उस पर वे विजय पाने में असफल हैं। आखिर वह गांव अंधकार को दूर
करने की कोशिश में पागल हो गया।
उस
गांव में एक यात्री भूला-भटका हुआ पहाड़ों पर किसी दूसरे गांव का पहुंचा, उस गांव
से निकला। उसने उस गांव की हालत देखी। वह हैरान हो गया। उसे विश्वास न आया कि
अंधकार को दूर करना भी इतनी कठिन बात है क्या? अंधकार से भी
हारने की कोई वजह, कोई कारण है क्या?
उसने
उस गांव के लोगों को कहा कि पागल हो तुम। अंधकार बहुत शक्तिशाली नहीं है। तुम
इसलिए नहीं हारते हो कि अंधकार शक्तिशाली है और तुम कमजोर हो। तुम हारते इसलिए हो
कि तुम अंधकार को सीधा हटाने का उपाय करते हो। अंधकार सीधा नहीं हटाया जा सकता है।
इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि अंधकार की कोई सत्ता, कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं
होता है। अंधकार तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। वह तो केवल प्रकाश की
एबसेंस है। उसका अपना कोई होना नहीं है कि तुम उसे हटा सको।
अंधकार
को मत हटाओ, प्रकाश को जलाओ। और प्रकाश जल आता है तो अंधकार कहीं भी नहीं पाया जाता
है। उसने दो पत्थरों से चोट की और प्रकाश को जलाकर उन्हें बताया। वे हैरान हो गए।
वे अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके कि जो बात इतनी कठिन थी, वह
इतनी सरल निकलेगी। प्रकाश आया और अंधकार नहीं था।
पता
नहीं यह कहानी कहां तक सच है। और सच हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन पूरी मनुष्य जाति अंधकार को दूर करने में लगी हुई है! और अंधकार को दूर करने
की इस चेष्टा में अंधकार तो दूर नहीं होता, प्रकाश भी उपलब्ध
नहीं होता--लेकिन मनुष्य जरूर दीन-हीन फ्रस्ट्रेटेड, मनुष्य
जरूर चिंतातुर, मनुष्य जरूर तनाव से भर जाता है और इस सीमा
तक यह बात पहुंच जाती है कि मनुष्य विक्षिप्त हो उठता है।
आज
हम करीब-करीब रुग्ण और विक्षिप्त हैं। और इस सारी विक्षिप्तता के पीछे, इस पागलपन
के पीछे, जिसमें मनुष्य जाति ग्रसित है--मनुष्य के इस चित्त
की रुग्णता के पीछे एक ही, एक ही बात काम कर रही है--वही जो
उस गांव में काम कर रही थी। हम अंधकार को दूर करने के प्रयास में संलग्न हैं।
प्रकाश को जलाने के प्रयास में नहीं--अंधकार को दूर हटाने के प्रयास में।
हर
मनुष्य अस्वस्थ,
बीमार और रुग्ण है चित्त के तल पर, क्योंकि वह
अंधकार को दूर करने की कोशिश में लगा है। अंधकार दूर नहीं किया जा सकता। इसका यह
अर्थ नहीं है कि अंधकार दूर नहीं हो सकता। अंधकार निश्चित ही दूर हो जाता है।
लेकिन प्रकाश के जलने से। सीधे अंधकार के साथ कुछ भी करने का उपाय नहीं है। वह है
ही नहीं, उसके साथ करने का उपाय होगा कैसे?
हम
सब एक निगेटिव,
एक नकारात्मक जीवन-विधि से पीड़ित हैं। अंधकार को दूर करने की विधि
से पीड़ित हैं। स्वभावतः हम अपने भीतर हिंसा दूर करना चाहते हैं; घृणा दूर करना चाहते हैं; क्रोध दूर करना चाहते हैं;
द्वेष, लोभ, मोह दूर
करना चाहते हैं;र् ईष्या दूर करना चाहते हैं। ये सब अंधकार
हैं। इनको दूर नहीं किया जा सकता सीधा। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है।
क्रोध, घृणा,
द्वेष यार् ईष्या किसी के अभाव हैं, किसी
प्रकाश की अनुपस्थिति हैं। स्वयं किसी चीज की मौजूदगी नहीं हैं। घृणा, प्रेम की अनुपस्थिति है। जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है। घृणा को
दूर नहीं किया जा सकता सीधा। न द्वेष को, नर् ईष्या को,
न हिंसा को। और जब हम इनको सीधा दूर करने में लग जाते हैं, तो अगर हम पागल न हो जाएं तो और क्या होगा। क्योंकि वे दूर नहीं होते।
उनको दूर करने की सारी कोशिश व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। और जब वे दूर नहीं होते तो
दो ही उपाय रह जाते हैं--या तो व्यक्ति पागल हो जाता है, या
पाखंडी हो जाता है। जब वे दूर नहीं होते तो उन्हें छिपा लेता है। ऊपर से जाहिर
करने लगता है वे दूर हो गए और भीतर, भीतर वे उबलते रहते हैं,
भीतर वे मौजूद रहते हैं, भीतर वे चित्त की
पर्तों पर सरकते रहते हैं। ऐसा दोहरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। एक जो ऊपर से
दिखाई पड़ने लगता है। और एक, एक जो भीतर होता है।
इस
द्वैत में इतना तनाव है,
इतनी अशांति है, इतनी कानफ्लिक्ट है। होगी ही,
क्योंकि जब एक आदमी दो हिस्सों में टूट जाएगा--एक जैसा वह है,
और एक जैसा वह लोगों को दिखलाता है कि मैं हूं।
मैंने
सुना है लंदन में एक बहुत अदभुत फोटोग्राफर था। उसने अपने स्टूडियो के सामने एक
तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर उसने लिख रखा था अपनी फोटो उतारने के दाम की सूची
लिख रखी थी। उस पर उसने लिख रखा था: जैसे आप हैं, अगर वैसा ही फोटो उतरवाना
है तो पांच रुपया। जैसे आप दिखाई पड़ते हैं, अगर वैसी फोटो
उतरवानी है तो दस रुपया। जैसा आप चाहते हैं कि दिखाई पड़ें, अगर
वैसी फोटो उतरवानी है तो पंद्रह रुपया।
एक
गांव का ग्रामीण पहुंचा। वह भी चित्र उतरवाना चाहता था। वह हैरान हुआ कि चित्र भी
क्या तीन प्रकार के हो सकते हैं। और उसने उस फोटोग्राफर से पूछा कि क्या पांच रुपए
को छोड़कर कोई दस और पंद्रह का फोटो भी उतरवाने आता है?
उस
फोटोग्राफर ने कहा,
तुम पहले आदमी हो, जो पांच रुपए वाला फोटो
उतरवाने का विचार कर रहे हो। अब तक तो यहां कोई पांच रुपए वाला फोटो उतरवाने नहीं
आया। जिनके पास पैसे होते हैं, वे पंद्रह रुपए वाला ही
उतरवाते हैं। मजबूरी, पैसे कम हों तो दस रुपए वाला उतरवाते
हैं। लेकिन मन उनका पंद्रह वाला ही रहता है कि उतरे तो अच्छा। पांच रुपए वाला तो
कोई मिलता नहीं। जो जैसा है, वैसा चित्र कोई भी उतरवाना नहीं
चाहता है।
हम
अपने व्यक्तित्व को ऐसी पर्त-पर्त ढांके हुए हैं। इससे एक पाखंड पैदा हुआ है। इस
पाखंड से सारा मनुष्य-चित्त रुग्ण हो गया है। और अगर कोई बहुत जिद्दी हो और अगर
कोई पाखंडी न होना चाहता हो और आग्रह करता रहे अंधकार को, घृणा को,
क्रोध को हटाने का, तो उसके लिए विक्षिप्त हो
जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं। वह पागल हो जाएगा।
सभ्यता
के बढ़ने के साथ-साथ पागलों की संख्या अकारण ही नहीं बढ़ती गई है। जितना सभ्य मुल्क, उतनी ही
पागलों की अधिक संख्या।
अमरीका
शायद सभ्यता में अग्रणी है,
इसीलिए सर्वाधिक पागल वहां होते हैं। और एक न एक दिन यह बात जब समझ
में आ जाएगी कि सभ्यता और पागलों का कोई अनिवार्य संबंध है तो आप पक्का समझ लें,
जिस मुल्क को पूरा सभ्य होना हो, उसे पूरा
पागल हो जाना पड़ेगा। या अगर कोई कौम बिलकुल पागल हो जाए तो समझ लेना कि वह सभ्यता
के शिखर पर पहुंच गई है।
यह
जो, अगर हम चित्त की बदलाहट की कोई गलत कीमिया, कोई गलत
केमिस्ट्री पकड़ लेंगे तो स्वभावतः चित्त विकृत हो जाएगा।
आज
की सुबह मुझे स्वस्थ चित्त के संबंध में ही थोड़ी बात करनी है। कल मैंने युवा, ताजा,
नया चित्त होना चाहिए इस संबंध में आपसे कुछ कहा था। दूसरे दिन की
सुबह, आज मैं, स्वस्थ-चित्त होना चाहिए,
इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि स्वस्थ चित्त न हो तो
सत्य की कोई अनुभूति संभव नहीं है।
लेकिन
स्वस्थ चित्त होना चाहिए,
इसे समझने के लिए, यह समझ लेना जरूरी है कि यह
चित्त अस्वस्थ कैसे हो गया ह? यह अनहेल्दी माइंड पैदा कैसे
हो गया? यह आदमी का चित्त इतना ज्वर-ग्रस्त, इतना विकृत इतना कुरूप कैसे हो गया? इतना अग्ली कैसे
हो गया? क्या बीमारी इस चित्त को लग गई है?
इस
चित्त को अंधकार को दूर करने की बीमारी लग गई है। एक बीमारी तो है अंधकार को दूर
करने की। और जब यह अंधकार दूर नहीं होता--जिसे हम बुरा कहते हैं, जिसे हम
पाप कहते हैं, जिसे हम अनीति कहते हैं--जब वह दूर नहीं होती
तो फिर क्या करे आदमी? फिर दो ही रास्ते हैं--या तो पागल हो
जाए, या पाखंडी हो जाए।
फिर
क्या करे?
तीसरा
रास्ता भी है एक। और वह यह कि वह किन्हीं आदर्शों की कल्पना में जो है उसे भूल जाए, एक एस्केप
ले ले, एक पलायन ले ले। हिंसक आदमी है, वह अहिंसा का आदर्श बना ले और अहिंसा की योजना और कल्पना में लीन हो जाए
और हिंसा को भूल जाए। क्रोधी आदमी है, वह क्षमा का आदर्श बना
ले, क्षमा की योजना में लग जाए कि कल मैं क्षमाशील हो जाऊंगा।
और कल की इस योजना में आज जो क्रोध है, उसे भूल जाए।
यह
तीसरा विकल्प भी मनुष्य के चित्त को अस्वस्थ करता है। क्योंकि तब उसके आज और कल
में एक तनाव,
एक टेंशन पैदा हो जाता है। वह कल की कल्पना में जीने लगता है और
असलियत में जीता है आज। जो आदमी कल अहिंसक होने का विचार कर रहा है कि मैं कोशिश
करके कल अहिंसक हो जाऊंगा, प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा, क्षमाशील हो जाऊंगा; वह आज क्रोधी है, हिंसक है। और हिंसक आदमी अहिंसक बनने की कोशिश भी करेगा, उस कोशिश में भी हिंसा मौजूद रहेगी।
इसीलिए
तथाकथित अहिंसक साधु-संन्यासी, साधक इतनी गहरी हिंसा में संलग्न होते हैं,
जिसका कोई हिसाब नहीं। यह जरूर बात सच है कि वे हिंसा दूसरे पर न
करके अपने पर ही करते हैं। हिंसा की धारा वे अपने पर ही लौटा लेते हैं। वे खुद के
ही विनाश में, खुद के ही डिस्ट्रैक्शन में संलग्न हो जाते
हैं। और किस-किस भांति वे अपने को पीड़ा देने लगते हैं, और
उन्हें खयाल भी नहीं होता कि यह सब हिंसा है। लेकिन वे अहिंसा की साधना के लिए यह
सब कर रहे हैं।
हिंसक
आदमी अहिंसक हो कैसे सकता है? वह जो कुछ भी करेगा उसमें हिंसा होगी। अहिंसा
की साधना भी करेगा तो हिंसा होगी। उसका माइंड तो वायलेंट है, वह तो हिंसक है। इसलिए जो भी वह मन करेगा, उसमें
हिंसा होगी। क्रोधी आदमी प्रेम की तैयारी करेगा तो उसमें भी क्रोध होगा। बातें
प्रेम की होंगी, पीछे क्रोध होगा।
मैंने
सुना है। एक क्रोधी बाप का बेटा घर छोड़कर भाग गया था। उसने अखबार में विज्ञापन
निकलवाया कि प्यारे बेटे,
तुम वापस आ जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारे प्रेम में बहुत दुखी है और
दिन-रात रो रही है। मैं खुद भी तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूं। शीघ्र
वापस लौट आओ। और अंत की पंक्ति थी कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा।
वह
सारी प्रेम की बातचीत--और शायद क्रोध में उसे खयाल ही न रहा कि अगर वापस न लौटे तो
चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो तुम चमड़ी उधेड़ोगे कहां, जब वह वापस ही नहीं लौटेगा?
लेकिन
लड़का फिर वापस नहीं लौटा। क्योंकि लड़के ने समझ लिया होगा कि न लौटने पर तो चमड़ी
नहीं उधेड़ी जा सकती,
लेकिन लौटने पर उसका उधेड़ा जाना निश्चित है।
यह
बिचारे का प्रेम कितने दूर तक जाएगा--ऊपर-ऊपर होगा। पीछे? पीछे वह
मौजूद है आदमी, जो वह है। हमारी सारी इन आदर्शों की बातचीत
में--प्रेम की, अहिंसा की, दया
की--भीतर हमारी हिंसा, हमारा क्रोध, हमारी
क्रूरता सब मौजूद होती है।
मैंने
सुना है एक सुबह एक पति अपना अखबार पढ़ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे अखबार पढ़ते देखकर
चिंता अनुभव की होगी। क्योंकि पत्नियां यह कभी पसंद नहीं करतीं कि उनका पति उनके
अतिरिक्त और किसी चीज में उत्सुक हो। अखबार में भी उत्सुक हो तोर् ईष्या पैदा होती
है। तो उस पत्नी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अब तुम मुझे प्रेम नहीं करते। मैं
आधे घंटे से बैठी हूं लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा नहीं, तुम अपना
अखबार ही पढ़े जाते हो। उसके पति ने कहा, गलती में हो तुम। अब
तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्रेम करता हूं। अब तो तुम्हारे बिना मैं एक क्षण
नहीं जी सकता। तुम्हीं मेरी श्वास, तुम्हीं मेरी प्राण हो।
और आखिर में कहा कि अब बकवास बंद करो, अब मुझे अखबार पढ़ने
दो। अब बहुत हो गया, अब बकवास बंद करो, अब मुझे अखबार पढ़ने दो!
एक
ऊपर, एक आवरण जीवन में हम प्रेम का ओढ़े बैठे रहते हैं। और पीछे? पीछे वह हमारी सारी क्रूरता और सारी हिंसा मौजूद होती है। अगर आदमी को जरा
खरोंच दो, उसका सारा झूठा व्यक्तित्व खतम और उसके भीतर से
असली आदमी बाहर। जरा किसी के पैर पर चोट लगा दो, जरा किसी को
धक्का दे दो--वह गई बात, वह जो ऊपर से आदमी था विलीन हो गया,
दूसरा आदमी मौजूद हो गया। इस आदमी का पता भी नहीं था कि यह इतनी ही
दूरी पर, पास ही मौजूद है।
हम
सब के भीतर वह आदमी मौजूद है। और उस आदमी की मौजूदगी और ऊपर से यह आवरण--झूठा, विरोधी--और
हमने इस विरोध को, भीतर हिंसा मालूम पड़ती है। तो जो अपोजिट
है, जो विरोधी है--अहिंसा, उसका वस्त्र
ओढ़ लिया। भीतर क्रोध है तो हमने ऊपर क्षमा का वस्त्र ओढ़ लिया। भीतर घृणा है तो
हमने ऊपर प्रेम का वस्त्र ओढ़ लिया।
आदमी
का चित्त विकृत है,
इस अपोजिट के कारण। यह जो विरोधी ओढ़े हुए है, इसके
कारण मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि इस विरोधी के ओढ़ने से वह जो भीतर है,
वह नष्ट नहीं होगा। बल्कि वह नष्ट हो सकता था, अगर यह विरोधी न ओढ़ा जाता। क्योंकि उसके साथ जीना बहुत कठिन था। उसके साथ
एक क्षण जीना कठिन था। इस विरोधी को ओढ़ लेने के कारण उसके साथ जीना आसान हो गया
है।
अगर
किसी भिखमंगे को यह खयाल हो जाए कि मैं सम्राट हूं--और ऐसा अक्सर भिखमंगों को खयाल
हो जाता है, तो फिर भिखमंगेपन के मिटने की कोई संभावना न रही। उसे तो खयाल है कि मैं
सम्राट हूं। वह आदमी भिखमंगा है, भिखारी है लेकिन खयाल है कि
मैं सम्राट हूं! तो अब उसके भिखमंगेपन के मिटने का क्या मार्ग रहा?
लेकिन
इस खयाल से वह सम्राट हो नहीं जाता है। रहता तो भिखमंगा ही है। एक सपना ओढ़ लेता है
सम्राट के होने का। और इस सपने ओढ़ लेने के कारण भिखमंगे में रहने की सुविधा मिल
जाती है। अगर यह खयाल न हो कि मैं सम्राट हूं और वह जाने कि मैं भिखारी हूं, तो भिखारी
होने के साथ जीना कठिन है। उसे बदलना होगा, उसे भिखारीपन से
छुटकारा और मुक्ति पानी होगी।
अगर
एक बीमार आदमी को खयाल हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं, तो फिर? फिर उसकी बीमारी के उपचार की क्या संभावना रही? वह
अपनी बीमारी को मिटाने के लिए क्या करेगा?
वह
कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इस खयाल से कि मैं स्वस्थ हूं, वह स्वस्थ
हो नहीं जाता है; रहता तो बीमार है। लेकिन इस खयाल के कारण
बीमारी को भीतर सरकने का, जीने का, मौका
मिल जाता है। बीमारी की मिटने की सारी संभावना समाप्त हो जाती है।
बीमारी
को मिटाने के लिए,
बीमारी को पूरी तरह जानना जरूरी है। बीमारी से मुक्त होने के लिए बीमारी
को भुलाना सबसे घातक बात है। और हम सब अपनी बीमारियों को भुलाकर बैठ जाते हैं। हम
सब तरकीबें निकाल लेते हैं कि बीमारी भूल जाए। और फिर बीमारी जीती है, भीतर सरकती है। अपरिचित और अनजान हो जाने के कारण, अनकांशस
हो जाने के कारण, अचेतन हो जाने के कारण, हमारा उससे ऊपर से कोई संबंध नहीं रह जाता, लेकिन
प्राणों को भीतर-भीतर वह रौंद डालती है। मनुष्य इसलिए अस्वस्थ है। मनुष्य का चित्त
इसलिए अस्वस्थ है।
इस
पूरी बात को अगर हम संक्षिप्त में समझें तो इसका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य तथ्यों को
छिपाने के लिए आदर्शों का उपयोग करता है। वह जो फैक्टस हैं, उनको
छिपाने के लिए फिक्शन खड़े करता है। जो तथ्य हैं, जो
सच्चाइयां हैं, उन्हें छिपाने के लिए झूठी कल्पनाएं और आदर्श
और आइडिअल्स खड़े करता है। और फिर इन आदर्शों के कारण तथ्यों को भूल जाता है। लेकिन
तथ्य हैं, वे भूलने से मिटते नहीं हैं।
अगर
कोई चीजें भूलने से मिटती होतीं, तब तो बहुत आसान बात थी। तब तो एक आदमी शराब पी
लेता और और दुख मिट जाता। लेकिन शराब पीने से दुख मिटता नहीं, केवल भूलता है। आदर्शों की शराब पी लेने से भी जीवन के तथ्य बदलते नहीं,
मौजूद रहते हैं।
यह
हमारा ही देश है,
यह अहिंसा की शराब हजारों साल से पी रहा है। लेकिन एक भी आदमी
अहिंसक नहीं हो पाया है। हिंसा मौजूद है। हमारे चित्त में सब तरफ हिंसा मौजूद है।
लेकिन हम अहिंसा की बातें करके अपनी हिंसा को छिपाए रखते हैं। जरा सी चोट और हमारे
हिंसा के फब्बारे निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारे कवि हिंसा के गीत गाने लगते हैं।
हमारे नेता हिंसा की बात करने लगते हैं। हमारे साधु-संन्यासी भी कहने लगते हैं,
अहिंसा की रक्षा के लिए अब हिंसा की बहुत जरूरत है। वह सारी अहिंसा
एक क्षण में विलीन हो जाती है। हम हजारों साल से प्रेम की बातें करते रहे हैं।
लेकिन हमारे जीवन में कहां है प्रेम? हम दया की, सेवा की बातें करते रहे हैं। कहां है दया और कहां है सेवा? और हमारी सारी सेवा और हमारी सारी दया भी हमारे गहरे से गहरे स्वार्थों की
अनुचर हो गई है।
एक
आदमी को मोक्ष जाना है,
इसलिए वह दया करता है, दान करता है। यह दया और
दान है, या कि सौदा है? एक आदमी को
आत्मा को पाना है, इसलिए वह सेवा करता है गरीबों की। यह सेवा
है, या अपने स्वार्थ के लिए गरीब को भी उपकरण बनाना है?
एक
चर्च में एक पादरी ने रविवार के दिन आने वाले बच्चों को समझाया कि जिन्हें भी
स्वर्ग जाना है,
उन्हें सेवा जरूर करनी चाहिए। उन बच्चों ने पूछा, हम कैसे सेवा करें, क्योंकि स्वर्ग तो हम सब जाना
चाहते हैं? उस पादरी ने कहा, कई प्रकार
हैं सेवा के। डूबता हुआ कोई हो तो उसे बचाना चाहिए। किसी घर में आग लग गई हो तो
जाकर घर का सामान या व्यक्तियों को बाहर निकालना चाहिए। या बहुत सरल सी बात,
कोई भी, किसी तरह का किसी को सहायता पहुंचानी
हो तो पहुंचानी चाहिए।
अगले
रविवार को जब वे बच्चे फिर आए तो उस पादरी ने पूछा, तुमने कोई सेवा का कार्य
किया? तीन बच्चों ने हाथ उठाए। एक बच्चे से पूछा, उसने क्या किया? उसने कहा, मैंने
एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। दूसरे से पूछा, उसने धन्यवाद
दिया कि खुश हूं मैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे
बच्चे से पूछा, तुमने क्या किया? उसने
कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। वह थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन फिर उसको भी
धन्यवाद दिया। और तीसरे से पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई।
वह
बहुत हैरान हुआ। उसने कहा,
क्या तीन बूढ़ी औरतें तुम्हें पार करवाने को मिल गईं। उन तीनों ने
कहा, तीन कहां, एक ही बूढ़ी औरत थी। तो
वह बहुत हैरान हुआ कि तुमको, तीन को उसे पार करवाना पड़ा! उन
तीनों ने कहा, वह पार होना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से पार करवाया। वह तो बिलकुल भागती थी--पकड़कर, बिलकुल जबर्दस्ती हमने पार करवाई। क्योंकि स्वर्ग जाना तो जरूरी है,
और सेवा करनी ही पड़ेगी।
उस
पादरी ने कहा,
अब कृपा करके ऐसी सेवा मत करना। अच्छा किया कि तुमने औरत को ही पार
करवाया। कहीं मकान में आग लगवाकर लोगों को नहीं बचाया। या किसी को नदी में डुबाकर
प्राण नहीं बचाए। यही बहुत है। अब तुम और सेवा मत करना।
सेवकों
ने दुनिया में ऐसे बहुत से काम किए हैं। लेकिन उन्हें सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि
स्वर्ग जाना जरूरी है। ये सारी सेवा, ये सारे दान, ये सारी दया, ये सारी अहिंसा की बकवास--हमारे भीतर
जो असली आदमी है, उसको छिपा लेती है। और वह जो असली आदमी है,
वही है। जो कुछ भी होना है, उसके द्वारा होना
है। जो भी जीवन में क्रांति या न-क्रांति, जीवन में कोई
परिवर्तन या न-परिवर्तन, जो कुछ भी होना है, उस असली आदमी से होना है, उस फैक्चुअल आदमी से,
जो मैं हूं, जो आप हैं।
यह
आदर्शों से कुछ भी होना नहीं है। लेकिन आदर्शों में हम अपने को छिपा लेते हैं। एक
बुरा आदमी अच्छे बनने की कोशिश में यह भूल जाता है कि मैं बुरा आदमी हूं। यही वह
भूलना चाहता है। यही वह भूलना चाहता है कि मैं बुरा आदमी हूं।
इसलिए
सब बुरे आदमी अच्छे आदर्शों को पकड़ लेते हैं। अच्छे आदर्श की जो बात करता
हो--पहचान लेना,
उसके भीतर बुरा आदमी मौजूद है। बुरा आदमी मौजूद न हो तो अच्छे आदर्श
की बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि तब आदमी अच्छा होगा, अच्छे
आदर्श का सवाल कहां है। अच्छा आदर्श भीतर छिपे हुए बुरे आदमी की तरकीब है और बहुत
गहरी तरकीब है, जिससे वह अपने को बचा लेता है।
अच्छे
बनने की कोशिश में बुरा आदमी भूल जाता है। और बुरा आदमी जब तक मौजूद है भीतर, तब तक कोई
अच्छा आदमी बन कैसे सकता है? वह लाख उपाय करे, वह जो भी करेगा, उसमें बुरा आदमी भीतर से लौटकर फिर
खड़ा हो जाएगा।
रोज
हम देखते हैं,
लेकिन शायद देखने की क्षमता हमने खो दी। बुरा आदमी भीतर मौजूद है,
वह हिंसा और घृणा से भरा हुआ चित्त--तो फिर आप कुछ भी करें, आप जो भी करेंगे, चाहे कितना ही पवित्र काम करें,
आपके पवित्रतम काम के पीछे भी चूंकि बुरा आदमी मौजूद है, आपका पवित्रतम काम भी धोखा होगा। उसके पीछे भी असलियत कुछ और ही होगी।
लेकिन
हो सकता है ऊपर से वह दिखाई पड़नी बंद हो जाए। शायद लोगों को दिखाई न पड़े। लेकिन
आपको भलीभांति दिखाई पड़ सकती है। और आपको दिखाई पड़ जाए तो आप स्वस्थ चित्त की दशा
में, स्वस्थ चित्त के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं।
पहली
बात है, स्वस्थ चित्त की दिशा में पहला कदम, पहला सूत्र इस
सत्य को देखना कि तथ्य में मैं क्या हूं? आदर्शों में नहीं।
फैक्चुअलिटि क्या है? मेरी आयाडियोलाजी क्या है, यह नहीं। आप क्या मानते हैं, यह नहीं। आप क्या हैं?
सच्चाई क्या है आपकी?
अगर
हम इसको जानने के लिए राजी हो जाएं--और इसको हम जानने को तभी राजी हो सकते हैं, जब यह
व्यर्थ खयाल हमारा छूट जाए कि आदर्शों की कल्पना और आदर्शों की दौड़ में हम बदल
सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। कभी कोई आदर्शों के द्वारा
परिवर्तित नहीं हुआ है। ऊपर से दिखाई भी पड़े कि यह आदमी बदल गया, भीतर वही आदमी मौजूद रहेगा।
एक
गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था। इतना क्रोधी था कि उसने अपनी पत्नी को कुएं में
फेंक दिया। उसकी पत्नी मर गई। पीछे उसे पश्चात्ताप हुआ होगा। सभी क्रोधी लोग पीछे
पश्चात्ताप जरूर कर लेते हैं। उस भांति उनका जो अपराध भाव है, समाप्त हो
जाता है। वे फिर से क्रोध करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। पश्चात्ताप
तरकीब है--किए गए बुरे से साफ कर लेने की स्वयं को।
उसने
पश्चात्ताप किया। उसने मित्रों से कहा कि मैं बहुत दुखी हुआ हूं। अब इस क्रोध से
मुझे किसी न किसी रूप में छुटकारा पाना है। हद हो गई। यह तो सीमा के बाहर चला गया।
जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था, उसी की मैंने हत्या कर दी। यह वाक्य कितना ठीक
लगता है कि जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था, उसी की मैंने
हत्या कर दी। लेकिन यह वाक्य क्या ठीक हो सकता है? क्योंकि
जिसको हम प्रेम करते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं? लेकिन हम रोज यह कहते हैं कि जिस बच्चे को मैं प्रेम करता था, उसको मैंने चांटा मार दिया। जिस मित्र को मैं प्रेम करता था, उससे मैंने बुरे शब्द बोल दिए। जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था, उससे मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा सच है, चांटा मारना सच
है, हत्या करना सच है--प्रेम का खयाल झूठा है।
लेकिन
उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हें पश्चात्ताप हो रहा है, यह बड़ी
अच्छी बात है। गांव में एक मुनि आए हुए हैं, तुम वहां चलो।
शायद उनसे तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। मुनि के पास उस क्रोधी व्यक्ति को ले गए।
और मुनि जो हमेशा से रास्ता बताते रहे हैं, पेटेंट, वह उन्होंने उसे बता दिया--कि तुम संन्यासी हो जाओ, बिना
संन्यासी हुए क्रोध इत्यादि से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार में रहोगे, तो तो क्रोध और लोभ और मोह में फंसे ही रहोगे। यह तो संसार में स्वाभाविक
है। संन्यासी हुए बिना क्रोध के बाहर तुम नहीं हो सकते हो।
वह
आदमी तो दुख में था ही। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए, वह नग्न खड़ा हो गया। उसने
कहा कि मैं संन्यासी हो गया। वह मुनि भी नग्न थे। मुनि बहुत हैरान हुए और बहुत
उन्होंने धन्यवाद किया उस व्यक्ति का कि ऐसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। इतना
संकल्पवान! तत्क्षण इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो जाने वाला! एक तो वह बाल्या भील
की कथा थी, एक दूसरी तुम्हारी है, उन्होंने
कहा।
लेकिन
मुनि धोखे में आ गए। और पूरे गांव ने भी प्रशंसा की। लेकिन उनको पता नहीं था, यह क्रोधी
आदमी का सहज लक्षण था। क्रोधी आदमी शीघ्रता से कुछ भी कर सकता है। वह उसके एंगर का
ही, वह उसके क्रोधी होने का ही सबूत था। संकल्प वगैरह का
सबूत नहीं था। और न ही उसके दृढ़ शक्ति वाले और विल पावर होने का सबूत था। वह सिर्फ,
उसके क्रोधी होने का सबूत था। जिस शीघ्रता से उसने पत्नी को कुएं
में धक्का दिया था, उतनी ही शीघ्रता से खुद को संन्यास में
धक्का दे दिया। ये दोनों एक ही चित्त के लक्षण थे।
लेकिन
गांव धोखे में आ गया। वह मुनि भी धोखे में आ गए। उन्होंने कई लोगों को संन्यास की
शिक्षा दी थी। लेकिन अब तक वे लोग कहते थे कि हां, कभी संन्यास लेंगे जरूर।
लेकिन इस आदमी ने तत्क्षण कपड़े फेंक दिए। गुरु के मन में भी शिष्य का बड़ा आदर हो
गया। और फिर उस शिष्य ने जो तपश्चर्या की, उसका तो पूरे देश
में कोई मुकाबला न रहा। उसने जैसे कष्टपूर्ण उपवास किए, वह
एक-एक पैरों पर घंटों खड़ा रहा। जैसे-जैसे कठिन उसने शीर्षासन किए; जितने उपद्रव हो सकते थे, सब उसने अपने साथ किए।
उसके तप की सब जगह प्रशंसा और हवा फैल गई। दूर-दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे
कि वह महातपस्वी, उसके तप का कोई प्रतियोगी न रहा।
लोग
फिर भी भूल में पड़ गए। उन्हें पता नहीं कि वही क्रोधी आदमी है। और यह क्रोध का ही
रूपांतरण है। यह क्रोध का ही रूप है कि वह आदमी आज धूप में खड़ा हुआ है, आज रेत
में लेटा हुआ है, कल कांटों पर सोया हुआ है, महीनों भूखा है, सूखकर हड्डी हो गया है। यह क्रोध का
ही रूप है। यह किसी को खयाल न आया। लोग कहने लगे महातपस्वी है! ऐसा तपस्वी नहीं
देखा गया था।
और
जितनी उसको प्रशंसा मिलने लगी, उतना अहंकार उसका मजबूत होने लगा। उतना ही वह
और तपस्या करने लगा। फिर तो उसकी ख्याति बहुत फैली। और जब किसी तपस्वी की ख्याति
बहुत फैल जाए तो वह राजधानी की तरफ यात्रा करता है। उसने भी यात्रा की। वह तपस्वी
राजधानी की तरफ चला। सभी तपस्वी अंततः राजधानी पहुंच जाते हैं। चाहे तप का कोई रूप
हो--धार्मिक कि राजनैतिक, कि समाज सेवा का। लेकिन तपस्वी अंत
में राजधानी जरूर पहुंचता है!
वह
भी राजधानी की तरफ चला। क्योंकि अब छोटे-मोटे गांव काम नहीं कर सकते थे। अब इस
तपस्वी के लिए,
महातपस्वी के लिए महा-राजधानी चाहिए थी।
वहां
राजधानी में उसके बचपन का एक मित्र, उसके साथ पढ़ा हुआ मित्र रहता था।
उसने सुनी प्रशंसा अपने इस मित्र की। वह उसके दर्शन को गया। मन में उसके संदेह
जरूर था कि वैसा क्रोधी व्यक्ति--कहीं यह सब क्रोध का ही रूपांतरण न हो? यह जो इतनी, इतनी तीव्र तपश्चर्या चल रही है,
यह कहीं क्रोध का ही रूप न हो? यह कहीं क्रोध
खुद पर ही न लौट आया हो? यह कहीं क्रोध धार्मिक न बन गया हो?
क्रोध
धार्मिक बन गया था। उसके मन में शक तो था। वह पहुंचा। सोचा था कि शायद अगर मित्र
सचमुच में ही साधु हो गया होगा तो कम से कम मुझे पहचान लेगा। बचपन में वर्षों वे
साथ रहे थे। लेकिन जो लोग भी अहंकार की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, वे फिर
किसी को भी पहचानते नहीं। सभी उनको पहचानें, यह तो वे चाहते
हैं। लेकिन किसी को उन्हें न पहचानना पड़े, ऐसा वे कभी नहीं
चाहते हैं। क्योंकि जो किसी को पहचानता है, वह छोटा हो जाता
है। और जो सबसे पहचाना जाता है, सब जिसे रिकग्नाइज करते हैं,
वह बड़ा हो जाता है।
देख
तो लिया मित्र को उसने,
लेकिन पहचाना नहीं। कौन पद पर पहुंचे लोग मित्रों को कब पहचानते हैं?
मित्र पास जाकर बैठ गया चरणों में। शक तो मित्र को हुआ कि मुझे
पहचान तो उन्होंने लिया है, क्योंकि वे तिरछी-तिरछी आंख से
देखकर इधर-उधर देखने लगते थे। क्योंकि न पहचाना होता तो बार-बार देखने की उस तरफ
जरूरत भी न थी। और देखने से बच भी रहे थे, उसकी भी कोई जरूरत
न थी।
उस
मित्र ने पूछा कि क्या महाराज मैं पूछ सकता हूं आपका नाम? महाराज ने
कहा, मेरा नाम! अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो
नहीं सुनते हो! मेरा नाम कौन है जो नहीं जानता! लेकिन फिर भी तुम पूछते हो! मेरा
नाम है मुनि शांतिनाथ।
कहने
से ही मित्र को खयाल आ गया कि शांति कितनी उपलब्ध हुई होगी। लेकिन दो-चार मिनट
शांतिनाथ आत्मा-परमात्मा की बातें करते रहे। फिर दो-चार मिनट के बाद उस मित्र ने
पूछा कि मुनि जी क्या मैं पूछ सकता हूं, आपका नाम क्या है? मुनि जी तो हैरान हो गए। हद हो गई! अभी इसने पूछा। बताया। कहा कि सुनते हो
या कि बहरे हो, कहा मैंने मुनि शांतिनाथ।
मित्र
का संदेह मजबूत होने लगा। शांति खो गई थी। दो-चार मिनट आत्मा-परमात्मा की फिर बात
चलती रही। मित्र ने फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम? उन्होंने डंडा उठा लिया! उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा
नाम। उसके मित्र ने कहा, मैं पहचान गया, शांतिनाथ जी। आप मेरे पुराने ही मित्र हैं, कोई फर्क
कहीं भी नहीं हुआ है।
चित्त
स्वयं को, सबको धोखा देने में समर्थ है। लेकिन धोखे से चित्त रुग्ण होता चला जाता है,
अस्वस्थ होता चला जाता है। हम सब भी ऐसे धोखे रोज दे रहे हैं। हमारी
मुस्कुराहटें झूठी, हमारा प्रेम झूठा, हमारी
दया झूठी, हमारी अहिंसा झूठी और भीतर हमारी जो सच्चाई है,
वह बिलकुल और। बाहर से हम मुनि शांतिनाथ हैं, भीतर
हम कौन हैं--वह हमें खोजना है और जानना है। वह हमें पहचानना है कि भीतर हम कौन हैं?
यह
जो बाहर का सारा का सारा हमने एक फिक्शन, एक कल्पना, एक
सपना खड़ा कर रखा है, एक आदर्श अपने ऊपर ओड़ रखा है--यही है,
जो हमारे जीवन में क्रांति को, ट्रांसफार्मेशन
को नहीं आने देता है। इसके कारण हम तथ्यों को देख ही नहीं पाते। तो फिर तथ्यों को
बदलने का सवाल कहां उठता है?
और, एक और
बहुत मजे की बात है कि तथ्यों को देखना ही, उनकी बदलाहट हो
जाती है। किसी तथ्य को पूरी तरह देख लेना ही उसकी बदलाहट हो जाती है। लेकिन तथ्य
की तीव्रता से हम दर्शन नहीं कर पाते तो बदलाहट नहीं हो पाती।
एक
वैज्ञानिक एक प्रयोग करता था। उसने दो बाल्टियों में पानी भरा और दो मेंढक पकड़कर
लाया। एक बाल्टी में उसने उबलता हुआ पानी भरा और मेंढक को उसमें छोड़ा। जानते हैं
आप क्या हुआ?
मेंढक छलांग लगाकर बाहर निकल गया। उबलता हुआ पानी था। क्या होता?
और होना क्या था? इतना तीव्र था उत्ताप जल
का--मेंढक दौड़ा, वह छलांग लगाकर बाहर निकल गया। इस बात का
दिखाई पड़ जाना मेंढक को कि आग सा पानी है--फिर कुछ करना थोड़े ही पड़ा। हो गई बात।
निकल गया बाहर।
दूसरी
बाल्टी में उसने मेंढक को डाला। उसमें कुनकुना पानी--ल्यूक-वार्म और धीरे-धीरे
बाल्टी को नीचे से वह गरम करता गया। मेंढक मर गया। धीरे-धीरे पानी गरम होता गया, धीरे-धीरे
पानी गरम होता गया। मेंढक को किसी तल पर यह पता नहीं चला कि पानी इतना गरम हो गया
है कि मैं निकल जाऊं। धीरे-धीरे पानी गरम हुआ, मेंढक एडजस्ट
होता गया। मेंढक जो था, वह धीरे-धीरे उस पानी से राजी होता
गया, वह धीरे-धीरे गरम होता गया--डिग्री, आधा-डिग्री गरम होता रहा। मेंढक भी उसके साथ तैयारी करता रहा और गरम होता
गया। मेंढक, थोड़ी देर में जब वह पानी उबला तो मेंढक उसी में
उबल गया और मर गया।
पहला
मेंढक छलांग लगाकर क्यों निकल सका? दूसरा मेंढक छलांग लगाकर क्यों
नहीं निकल सका?
दूसरे
मेंढक को पानी के गरम होने का तथ्य तीव्रता से दिखाई नहीं पड़ सका। धीरे-धीरे पानी
गरम होता गया,
वह एडजस्ट होता गया और अंत में मर गया।
जो
अहिंसक दिखाई पड़ते हैं,
वे अपनी हिंसा को कभी नहीं देख पाते अहिंसा के कारण। उनके भीतर की
हिंसा ल्यूक-वार्म मालूम पड़ने लगती है, कुनकुनी मालूम पड़ने
लगती है। वे रोज छानकर पानी पी लेते हैं। रात भोजन नहीं करते हैं। मांस नहीं खाते
हैं। ऐसे वे अहिंसक हो जाते हैं। भीतर की हिंसा कुनकुनी मालूम पड़ने लगती है। लेकिन
अगर वे अहिंसा की इस सारी बातचीत को अलग कर दें और पूरी दृष्टि से भीतर की हिंसा
को देखें तो जैसे मेंढक छलांग लगाकर बाहर निकल गया, वैसे ही
मनुष्य हिंसा के बाहर निकल सकता है। वैसे ही मनुष्य दुख के भी बाहर निकल सकता है।
वैसे ही मनुष्य अज्ञान के भी बाहर निकल सकता है।
लेकिन
हमारे आदर्श हमारे जीवन को कुनकुना बना देते हैं। और जो आदमी अपने जीवन को जितना
आदर्शों से घेर लेता है,
उतना ही उसके जीवन में ट्रांसफार्मेशन, वह
क्रांति का क्षण कभी भी नहीं आ पाता, जो जीवन को बदल दे और
नया कर दे।
अस्वस्थ
चित्त है आदर्शों के कारण। लेकिन हम तो यही सोचते रहे हैं हजारों वर्षों से कि
आदर्शों के कारण ही हम मनुष्य हैं! पशु नहीं हैं, फलां नहीं हैं, ढिकां नहीं हैं! आदर्श ही हमारे जीवन का लक्ष्य हैं। आदर्श जिसके जीवन में
है, वही महान है! आदर्श जिसके जीवन में है, वही नैतिक, वही धार्मिक है!
झूठी
हैं ये सब बातें। आदर्श जिसके जीवन में है, वह कभी धार्मिक हो ही नहीं सकेगा।
आदर्श खुद को धोखा देने का, सेल्फ डिसेप्शन की तरकीब है,
साइंस है। और हजारों साल से आदमी अपने को धोखा दे रहा है। इस
प्रवंचना को तोड़ना जरूरी है।
जिस
व्यक्ति को भी स्वस्थ चित्त उपलब्ध करना हो, उसे आदर्शों के जाल से मुक्त हो ही
जाना चाहिए। फिर हम जीवन के तथ्यों को जैसे वे हैं, देखने
में समर्थ हो सकते हैं। फिर हम अपने भीतर उतर सकते हैं और खोज सकते हैं--हिंसा को,
क्रोध को, घृणा को।
स्वास्थ्य
तो आधा इससे ही उपलब्ध हो जाएगा, जिस क्षण आपके आदर्शों से चित्त मुक्त हो गया।
आप एकदम सरल हो जाएंगे। एक ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता आ जाएगी।
आदर्श की वजह से एक दंभ आ जाता है--मैं अहिंसक हूं, मैं फलां
हूं, मैं ढिकां हूं, मैं धार्मिक
हूं--ये सब अहंकार के रूप हैं, रोग हैं।
लेकिन
जो आदमी सारे आदर्शों को मन से हटा देता है, और मन की तथ्यात्मकता को, वह जो मन है--हिंसा, क्रोध, घृणा
से भरा हुआ,र् ईष्या से भरा हुआ--उसको जानता है वह एकदम
विनम्र हो जाता है। एक ह्यूमिलिटि अचानक उसके ऊपर आ जाती है। वह देखता है, मैं क्या हूं? तथ्य बताते हैं कि मैं क्या हूं?
मेरी असलियत क्या है? और जिस दिन वह पूरी
शांति से और पूरी सरलता से, पूरी विनम्रता से इन तथ्यों को
देखता है--वह देखना ही, वह दर्शन एक छलांग बन जाती है--एक
जंप, उसके जीवन में आ जाता है, एक
क्रांति उसके जीवन में आ जाती है।
कैसे
हम उन तथ्यों को देख सकेंगे, उसकी बात तो कल सुबह मैं करूंगा।
अभी
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदर्शों के कारण हम नहीं देख पाते हैं। आदर्शों के
कारण एक भ्रमजाल,
एक इलूजन पैदा हो जाता है। और हम सब आदर्शों में पाले गए हैं और जी
रहे हैं। इससे एक हिपोक्रेसी, एक पाखंड, एक झूठ, एक वंचना खड़ी हो गई है। और वही झूठ, वही वंचना, वही स्वयं को कुछ और समझना--जो कि हम हैं,
उससे भिन्न, उससे विरोधी--वही वंचना हमारे
जीवन का सारा स्वास्थ्य है।
एक
युवक सारी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हुआ था। उस विस्तृत यात्रा में एक
अनजान-अपरिचित रास्ते पर एक फकीर से उसका मिलना हो गया। वह फकीर भी अपने गांव को
लौटता था। वह युवक जिस देश से आता था, उस देश के सभी लोग सफेद कपड़े पहनते
थे। और यह फकीर बड़ा अजीब मालूम पड़ा। यह पूरे ही काले कपड़े पहने हुए था। तो उस युवक
ने उस फकीर से पूछा कि आप एकदम काले कपड़े पहने हुए हैं। हमारे देश में तो सभी लोग
सफेद कपड़े पहनते हैं। उस फकीर ने कहा, सफेद कपड़े पहन सकूं
ऐसा अभी मेरा मन कहां? मन है मेरा काला, इसलिए काले कपड़े पहने हुए हूं।
वह
युवक बोला, तब तो सफेद बिलकुल ही पहनने चाहिए। और अगर खादी के मिल जाएं तो और भी
अच्छा। क्योंकि काला मन हो तो सफेद कपड़े में छिप जाता है। और खादी के हों, तब तो सोने में सुगंध आ जाती है।
हमारे
मुल्क में तो लोग ऐसी नासमझी कभी नहीं करते कि कोई काला कपड़ा पहनता हो और काले
चित्त का आदमी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता।
उस
फकीर ने कहा,
लेकिन मैं दुखी हूं। मैं वही कपड़े पहनना चाहता हूं, जो मैं हूं। क्योंकि सफेद कपड़े पहनने से तुम्हें धोखा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो धोखा नहीं होगा। मैं तो जानूंगा। और सफेद कपड़ों के कारण और
भी जानूंगा कि भीतर, भीतर सब काला है।
उस
युवक ने कहा कि किस गांव में आप रहते हैं? मैं वहां जरूर आना चाहूंगा। और
संभव है, अपनी यात्राओं में वहां से मैं निकलूं। तो मैं आपके
दर्शन करने आना चाहूंगा। किस मोहल्ले में आप रहते हैं?
उसने
कहा, तुम पूछ लेना मेरे गांव में आकर कि झूठों की बस्ती कहां है। मैं वहीं रहता
हूं।
झूठों
की बस्ती! उस युवक ने कहा हद हो गई। ऐसा नाम हमने सुना नहीं। हजारों बस्तियां हैं
हमारे देश में,
हजारों मोहल्ले, हजारों नगर, हजारों गांव। हमारे यहां तो ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोई झूठों की भी
बस्ती हो। हमारे यहां तो जिस मोहल्ले में लोग एक-दूसरे की गर्दन काटने को तैयार
रहते हैं, उसका नाम शांति नगर रखते हैं। और जिस मोहल्ले में
हर आदमी एक-दूसरे की जेब में हाथ डाले रहता है, उसका नाम सर्वोदय
नगर रखते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कभी हमने सुना नहीं। क्या कहते हैं, झूठों की बस्ती!
लेकिन
उसने कहा, हां, मेरी बस्ती का तो यही नाम है। आओ तो पूछ लेना।
वह
युवक लंबी यात्राओं में उस गांव में पहुंचा। उसने गांव में जाकर बहुत लोगों को
पूछा कि झूठों की बस्ती कहां है। गांव के लोगों ने कहा, पागल हो
गए हो? ऐसे तो सारी दुनिया ही झूठों की बस्ती है, लेकिन नाम कौन रखेगा अपनी बस्ती का, झूठों की बस्ती।
उसने
कहा, एक फकीर था काला कपड़ा पहने हुए। तो किसी ने कहा, हां,
ऐसा एक फकीर है इस गांव में। लेकिन वह झूठों की बस्ती में नहीं,
वह तो मुर्दों की बस्ती में रहता है, मरघट में
रहता है। तुम्हें मालूम होता है कोई भूल हो गई। उसने कहा होगा मुर्दों की बस्ती,
तुम झूठों की बस्ती के खयाल में आ गए। तुम पूछो मरघट कहां है। मरघट
पर एक फकीर रहता है इस गांव में, जो काले कपड़े पहनता है।
खैर, वह खोजता
हुआ मरघट पहुंचा और बात सच निकली। वह मरघट पर फकीर का झोपड़ा था। फकीर के पास
जाकर...वह अंदर गया तो देखा बड़ी हड्डियां, बड़े सिर, खोपड़ियां, उस झोपड़े में चारों तरफ रखी हुई हैं,
ढेर लगा हुआ है, और फकीर बीच में बैठा हुआ है।
उसने कहा कि आप तो मुझसे कहे थे कि मैं झूठों की बस्ती में रहता हूं और आप तो यहां
मुर्दों की बस्ती में रहते हैं। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। पूछते-पूछते हैरान हो
गया।
उस
फकीर ने कहा,
दोनों ही बातें सच हैं। इन मुर्र्दों की खोजबीन करने से मुझे इस
बस्ती का नाम झूठों की बस्ती रखना पड़ा। कैसी खोजबीन? तुम
देखते हो, ये हड्डियां और खोपड़ियां रखी हैं। मैंने ब्राह्मण
की खोपड़ी को बहुत खोजबीन की कि पता चल जाए शूद्र की खोपड़ी से भिन्न है। लेकिन कुछ
पता नहीं चलता। मैंने साधु की हड्डियां खोजीं और असाधु की, और
दोनों में बहुत पता लगाया कि कोई फर्क पता चल जाए। फर्क पता नहीं चलता। और ये सारे
लोग जब तक जिंदा थे, तब तक ये बहुत फर्क मानते थे कि मैं यह
हूं, तुम वह हो। और मरने पर मैं पाता हूं कि सब मिट्टी साबित
हुए। और एक ने भी जिंदगी में यह नहीं कहा कि मैं मिट्टी हूं। इसलिए मैंने इनकी
बस्ती का नाम झूठों की बस्ती रख दिया है।
सब
झूठे थे। असलियत मिट्टी थी। लेकिन न मालूम क्या-क्या दावे करते थे कि मैं यह हूं, मैं वह
हूं। मैं ब्राह्मण हूं, तू शूद्र है। मैं नेता हूं, तू अनुयायी है। मैं गुरु हूं, तू शिष्य है। फलां हैं,
ढिकां हैं--न मालूम क्या। असलियत एक थी कि सब मिट्टी थे। मरघट पर
आकर मुझे यह पता चला, इसलिए मैंने इसका नाम झूठों की बस्ती
रख ली।
और
शायद तुम्हें हैरानी होगी कि मरघट को बस्ती कहना उचित है या नहीं। तो मैंने इसलिए
इसका नाम बस्ती रखा है कि जिसको तुम बस्ती कहते हो, वहां तो रोज कोई न कोई मरता
है और उजाड़ हो जाती है। यहां जो एक दफे बस जाता है, फिर कभी
नहीं उजड़ता। इसका नाम मैंने बस्ती रख छोड़ा है। और ये सब झूठे थे, मरने से यह पता चल गया।
हम
सब भी झूठे लोग हैं। और जब तक हम झूठे लोग हैं, तब तक हम अस्वस्थ रहेंगे। हम
स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए झूठ से मुक्त होना जरूरी है।
किस
झूठ से?
वह
जो हमने अपने व्यक्तित्व के संबंध में सृजन कर रखी है, निर्माण
कर रखी है। इस झूठ से मुक्त होना जरूरी है, जो हमने अपने
बाबत आदर्शों का जाल खड़ा करके निर्मित कर ली है। और जो इस झूठ से मुक्त नहीं होता,
उसका सत्य से कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। व्यक्तित्व झूठा हो तो
सत्य से मिलन कैसे होगा? सत्य से मिलने के लिए कम से कम
सच्चा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। कम से कम सच्चाई तो साफ होनी चाहिए कि मैं क्या
हूं।
तो
आज की सुबह तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यह भ्रम-जाल, जो हमने आदर्शों का अपने
आसपास खड़ा कर रखा है--उस भ्रम-जाल में हम झूठे आदमी हो गए हैं। और हमारी दुनिया
झूठों की बस्ती हो गई है।
कैसे
इसको हम देख सकें--उस देखने की प्रक्रिया के लिए कल सुबह मैं आपसे बात करूंगा। अब
हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे।
सुबह
के ध्यान के संबंध में दो बातें आपसे कह दूं फिर हम बैठें।
रात
हमने ध्यान किया। उसमें हम लेट गए थे। सुबह के इस ध्यान में हम बैठे रहेंगे अपनी
जगह। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शरीर को सीधा रखकर, लेकिन
सीधा रखने में कोई तनाव न पड़े। बहुत आहिस्ता से, आराम से।
सारे शरीर को ढीला भी छोड़ देना है, ताकि शरीर पर कोई किसी
तरह का स्ट्रेन न हो। ऐसे बैठ जाना है, जैसे हम विश्राम कर
रहे हैं। फिर बहुत आहिस्ता से आंख बंद कर लेनी है। वह भी बहुत आहिस्ता से। आंख पर
भी जोर न पड़े कि हमने आंख भींचकर बंद कर ली हो--पलक गिर जाए।
फिर
क्या करेंगे?
फिर
कुछ भी नहीं करेंगे। चुपचाप बैठे रहेंगे। जस्ट सिटिंग, कुछ भी
नहीं करना है।
वह, जापान में
तो ध्यान के लिए कहते हैं--झाझेन। और झाझेन का मतलब होता है: जस्ट सिटिंग, बस खाली बैठे रहना।
एक
बहुत बड़ा आश्रम था जापान में। और जापान का बादशाह उस आश्रम को देखने गया। कोई हजार
भिक्षु उस आश्रम में रहते थे। आश्रम का जो प्रधान था भिक्षु, उसने
बादशाह को सभी जगह दिखलाईं। जाकर दिखलाया एक-एक झोपड़ा--यहां भिक्षु स्नान करते हैं,
यहां भोजन करते हैं, यहां अध्ययन करते हैं।
बीच में एक विशाल भवन था--राजा बार-बार पूछने लगा और वहां क्या करते हैं? भिक्षु उसकी बात सुनकर चुप रह जाता था। राजा बहुत हैरान हुआ। बाथरूम,
पाखाने सब बतलाए। लेकिन वह जो विशाल भवन था, जो
देखने जैसा लगता था, उसकी वह भिक्षु बात भी नहीं करता था।
आखिर
राजा के विदा का वक्त आ गया। द्वार पर लौट आया, अभी वह भवन नहीं दिखलाया गया था।
राजा ने कहा, या तो मैं पागल हूं, या
तुम। जिसे मैं देखने आया था, वह भवन तुम दिखलाते नहीं। और
फिजूल के झोपड़े मुझे दिखलाते फिरे। अब मैं जा रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं,
वहां क्या करते हो?
उस
भिक्षु ने कहा,
तुम्हारे इस पूछने के कारण ही मैं बताने में असमर्थ हो गया। वहां हम
कुछ नहीं करते। वह हमारा ध्यान का कक्ष है। वहां हम कुछ भी नहीं करते। तुम बार-बार
पूछते हो, वहां क्या करते हो? तो मैं
वे झोपड़े तुमको बताता रहा, जहां हम कुछ करते हैं। कहीं स्नान
करते हैं, कहीं भोजन करते हैं। इस भवन में हम कुछ भी नहीं
करते। तो अब मैं कैसे बताऊं कि हम वहां क्या करते हैं? इसलिए
मैं ले नहीं गया। मैं समझ गया कि यह करने की भाषा समझता है, न
करने की भाषा समझेगा नहीं। इसलिए मैंने उस भवन को छोड़ दिया। वहां हम कुछ भी नहीं
करते। वहां तो हम बस बैठ जाते हैं। कुछ भी नहीं करते।
तो
यहां भी हम बस बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आवाजें सुनाई पड़ेंगी, हवाएं
पत्तों को हिलाएंगी, वृक्षों से आवाज होगी, उस आवाज को चुपचाप सुनते रहेंगे।
आज इतना ही।
साधना-शिविर, माथेरान, दिनांक
२०-१०-६७, सुबह

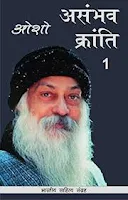
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें